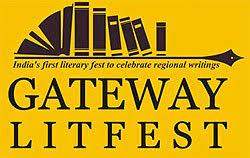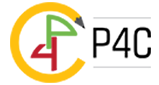साहित्य में अन्वेषण का आधार भिन्न-भिन्न होता है। अब यहां यह बात स्पष्ट करनी जरूरी है कि यह आधार हमेशा भौतिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक, वर्गीय व राष्ट्रीय भी होता है।
प्रासंगिकता के दार्शनिक और वर्गीय आधार उस समय और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब उनका साबका आलोचनात्मक दृष्टिकोण व व्याख्याओं से पड़ता है। इसकी वजह यह है कि कोई भी आलोचक, चाहे वह अध्यापक हो, व्याख्याकार अथवा विश्लेषक- इस वर्ग समाज का ही उत्पाद है। अपने जन्म, लालन-पालन के कारण हर बच्चा एक खास वर्ग के दायरे में आता है। शिक्षा के जरिए बच्चे को उस प्रभुत्वकारी वर्ग की संस्कृति, मूल्य व विश्वदृष्टि से लैस किया जाता है जो उसके परिवार से मेल खाती हो या न खाती हो। अपने जीवन के वर्ग संघर्षों में वे यह या वह पक्ष ले सकते हैं- इसके लिए उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए साहित्य, संस्कृति और इतिहास की उनकी व्याख्या उनके दार्शनिक दृष्टिकोण अथवा बौद्धिक आधार और उनके चेतन या अवचेतन में बसे वर्ग सहानुभूतियों से प्रभावित होगी।
एक रिसर्चर या आलोचक जो वास्तविक जीवन में उन लोगों के प्रति संदेह करता है जो मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वह उन चरित्रों पर भी संदेह करेगा जो मुक्ति के लिए संघर्षरत हैं- भले ही वे पात्र किसी कविता या उपन्यास के क्यों न हों। अगर कोई रिसर्चर या आलोचक वास्तविक जीवन में वर्गों, वर्ग-संघर्ष, साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आदि विषयों पर ऊब महसूस करता है तो उस कला कृति में भी ऊब महसूस करेगा, जहां ऐसी थीम हो। सर्जनात्मक लेखन की तरह आलोचनात्मक व शोधात्मक क्षेत्र में विचार का द्वंद्व रहेगा। किसी आलोचक का विश्व दृष्टिकोण क्या है, वह किन मूल्यों के साथ है अथवा किस वर्ग के प्रति उसकी हमदर्दी है- इस बात का असर किसी कविता या उपन्यास की व्याख्या पर पड़ेगा तथा किसी रचनाकार की रचनाओं के मूल्यांकन में भी वह वही बात रखना चाहेगा।
हम जो साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति, धर्म, मैनेजमेंट के प्रश्नों से जुड़े हैं- चाहे अध्यापक या रिसर्चर या छात्र के रूप में उन्हें यह बात हमेशा महसूस करनी चाहिए कि उन्होंने संघर्ष को सामान्य ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद की और न्याय को एक आवेग दिया। कोई भी साहित्य तब तक बेमानी है, जब तक वह स्वतंत्र आम आदमी की असीम रचनात्मक क्षमता को अधिक से अधिक उच्च स्तर तक पहुंचाने के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध न हो।
भारत के विश्वविद्यालयों में हम जो साहित्य पढ़ाते व शोध करते हैं, उसे हमारे इतिहास की भव्यता को अभिव्यक्त करना चाहिए। जो साहित्य हमारे पाठ्य विषय को सुशोभित करता हो, उसका चयन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह बाधक सामाजिक सरंचनाओं के खिलाफ हमारे संघर्ष की दृष्टि से कितना प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए एक ऐसे उपन्यास का चयन करें। समकालीन समाज की पतनशीलता तथा उसके माध्यम से संस्कृति में आ रहे बदलावों का गहरा विश्लेषण करना संभव हो। अब इसमें हमारी पूर्व कही गई बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि शोध व व्याख्या में दृष्टि की भूमिका अहम् हो जाएगी।
ऐसा करके हम अपने छात्रों के अंदर एक आलोचनात्मक मानसिकता विकसित कर पाएंगे। उन्हें ऐसा बना सकेंगे जो भारत में अपने समग्र परिवेश का आलोचनात्मक ढंग से आकलन और मूल्यांकन कर सकें और इस प्रक्रिया में हासिल उपकरणों की मदद से दूसरी दुनिया का आकलन और मूल्यांकन कर सकें। साहित्य में दो तरह के परस्पर विरोधी सौंदर्यबोध होते हैं, दमन व उत्पीडऩ तथा साम्राज्यवाद के प्रति मौन स्वीकृति का सौंदर्यबोध।
अनेक बार ऐसा देखा गया है कि विश्वविद्यालय में साहित्य का अध्यापन ऐसे अध्यापक से कराया जाता है जो साहित्य की बारीकियों में प्रशिक्षित नहीं होते तथा वे किसी भी साहित्य का चाहे वह भारत का हो या भारत के बाहर का, ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सकते। इस प्रकार वे अपने भाषा-ज्ञान तथा साहित्य के प्राकृतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि से अपने परिचय की ओट में अपने अज्ञान को छुपा लेते हैं।
इस प्रकार हम पाते हैं कि साहित्य के शोधार्थी व अध्यापक तथा छात्र के लिए आत्म पहचान का रास्ता भारतीय विरासत व संस्कृति से होकर गुजरना चाहिए। शोध का साहित्य में अर्थ है- शाब्दिक बिम्बों के रूप में जनता के उन संघर्षों की रचनात्मक चेतना को अभिव्यक्ति देना, क्योंकि साहित्य किसी देश की जनता के जीवन को अभिव्यक्ति देता है।
हम साहित्य में शोध के माध्यम से यह देख सकते हैं कि देश के सामने इस साहित्य के माध्यम से कौन से बिंब प्रस्तुत हो रहे हैं? औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली में ‘वर्नाकुलर’ यानी देशी भाषाओं का उचित स्थान नहीं होता। उनके साहित्य को संभ्रांत लोगों में वह स्थान नहीं होता, जो यूरोपीय भाषाओं के साहित्य का होता है। साहित्य पर शोध करते हुए यह सांस्कृतिक द्वंद्व स्वत: दीख पड़ेगा। मैं एक भोजपुरी का साहित्यकार व आलोचक हूं। इस भाषा के साहित्य को इस मल्टीनेशनल युग में काफी संघर्ष झेलना होता है।
कोई भी संस्कृति सही व गलत, अच्छी व बुरी, सुंदर व असुंदर जैसी ढेर अवधारणाओं की वाहक व संप्रेषक होती हैं, जिन्हें मानवीय समझा जाता है। कई बार सत्ता व संस्कृति में जनतांत्रिकता, गड्डमड्ड करने लगती है। औपनिवेशिक शिक्षा एक अभिजात देशज वर्ग तैयार करती है, जिसने साम्राज्यवादी संस्कृति को आत्मसात कर लिया हो, जिसके जरिए साम्राज्यवाद अपनी नई औपनिवेशिक अवस्था में देश की संपदा की लूट जारी रख सके।
किसान समुदाय व निम्न वर्ग ने अपने नए लेखक तैयार किए, जो भाारतीय भाषाओं में लिखते रहे हैं। शोध के विभिन्न स्तरों पर किसान के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक द्वंद्वों का पता चलता है। अभी तक मेरी जानकारी में हिन्दी या भोजपुरी में किसानों की आत्महत्या पर बेहतर सर्जनात्मक समूची पुस्तक नहीं आई है [ एकाध अपवाद छोड़ कर ] ! शोधार्थी पता लगाएं कि इतनी बड़ी समस्या पर कुछ रचनाओं को छोडक़र समग्रता में कुछ क्यों नहीं आया ?
लिखित साहित्य की अनेक रचना बरीकियां मौखिक साहित्य के स्रोतों से आती हैं। इसलिए यह एक नए शोध के रूप में देखा जाना चाहिए कि मौखिक साहित्य की जीवंतता का लिखित साहित्य पर किन रूपों में असर पड़ता है। असल में सारी बहस दिशा के बारे में है, साहित्य के अध्यापन-अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में है, साहित्य के साथ-साथ आज भारत में किस तरह का इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा कलाओं की शिक्षा दी जाए, इस बारे में है। इसलिए शोध में यह ध्यान रखना चाहिए-
>> जनता का साहित्य जनता की विश्वदृष्टि को परिभाषित और उद्घाटित करने का अनिवार्य अंग है। ध्यान रखें कि ध्यान न देने पर औपनिवेशिकता का सूक्ष्म प्रवेश संभव है।
>> एक नवाचारी शोध इस बात की पड़ताल करता है कि कोई समाज अपने साहित्य व संस्कृति का अध्ययन पहले करे, फिर अन्य समाजों की संस्कृति व परिवेश के संदर्भ में इसे देखें।
>> हमारा साहित्य सकारात्मक व रचनात्मक क्षमता से युक्त जनता के आत्मसंघर्ष की प्रक्रिया को कितना संबल देता है।